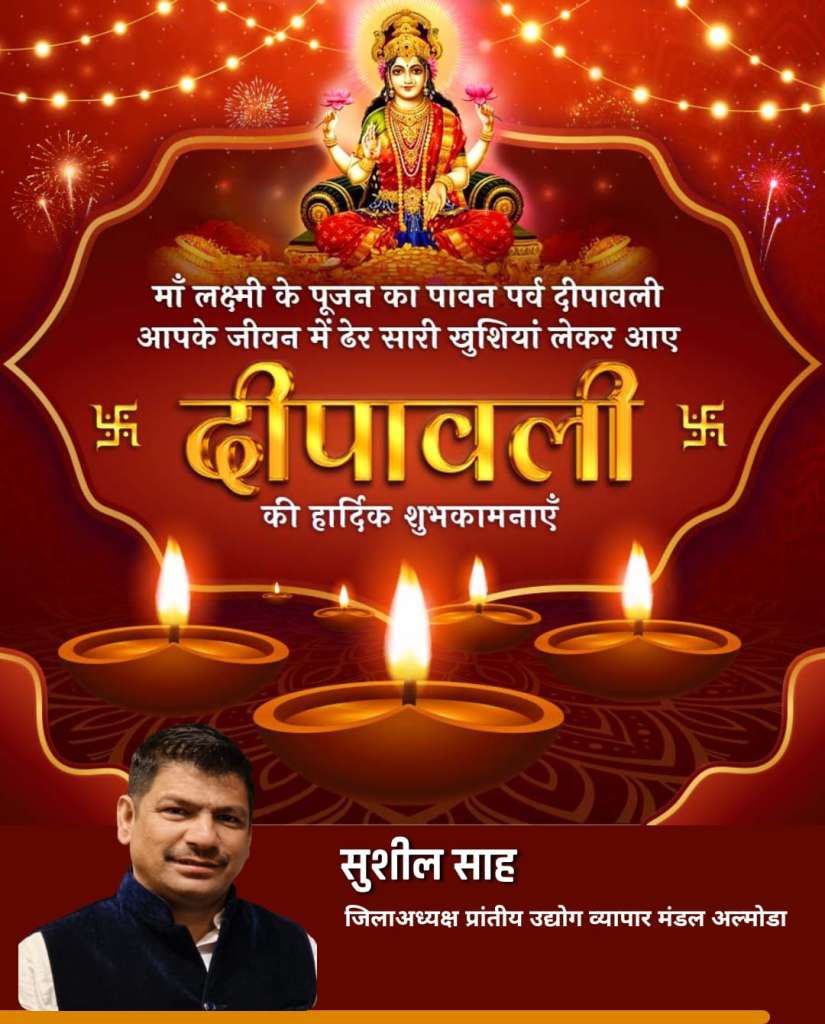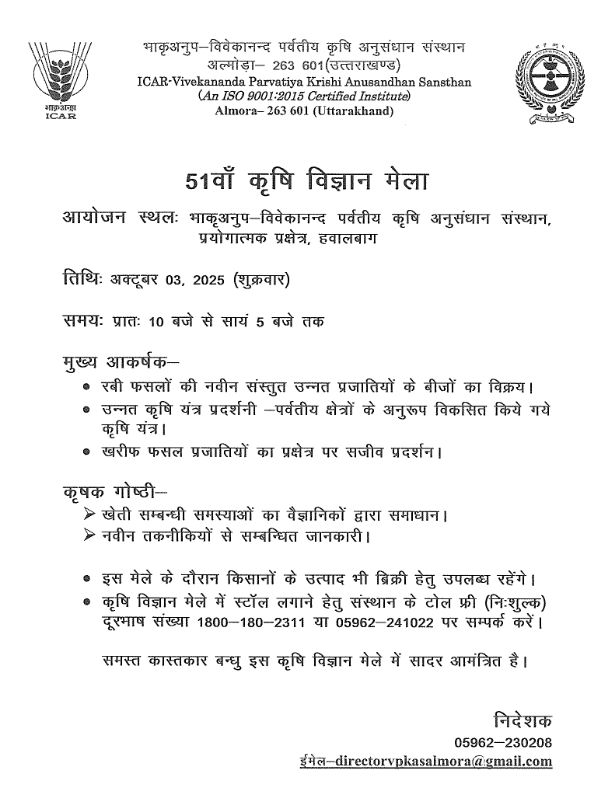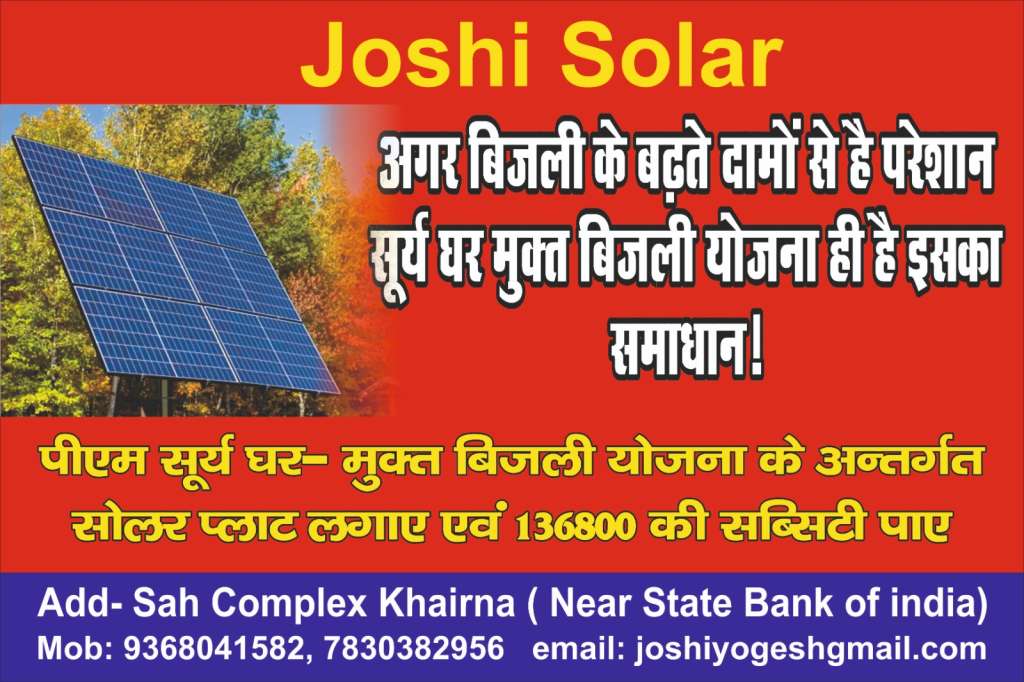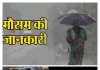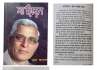उत्तराखंड, जिसे “देवभूमि” के नाम से जाना जाता है, अपनी हिमालयी गोद में बसी प्राकृतिक सुंदरता, पवित्र नदियों और समृद्ध जैव विविधता के लिए विश्वविख्यात है। हालांकि, पिछले कुछ दशकों से जलवायु परिवर्तन नामक एक अदृश्य दुश्मन इसकी प्राकृतिक धरोहर और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। यह संकट न केवल पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, बल्कि सीधे तौर पर राज्य की अर्थव्यवस्था, कृषि और लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रहा है।
प्रमुख कारण और उनके प्रत्यक्ष प्रभाव
जलवायु परिवर्तन के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्राकृतिक हैं, लेकिन अधिकांश मानवजनित हैं। हिमालय का वायुमंडल वैश्विक औसत की तुलना में कहीं अधिक तेजी से गर्म हो रहा है, जिसे ‘हिमालयी ताप प्रवर्धन’ (Himalayan Warming) कहा जाता है। इसका मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन (कोयला, पेट्रोल) के जलने से उत्सर्जित होने वाली हानिकारक ग्रीनहाउस गैसें (जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन) हैं।
- ग्लेशियरों का पिघलना: बढ़ते तापमान के कारण हिमालय के ग्लेशियर, जो एशिया की प्रमुख नदियों (गंगा, यमुना) के मुख्य जल स्रोत हैं, अभूतपूर्व गति से पिघल रहे हैं। इससे नदियों में अचानक बाढ़ आ सकती है और भविष्य में जल संकट पैदा हो सकता है।
- अनियमित वर्षा और मौसम चक्र: पारंपरिक मौसमी चक्र बाधित हो रहा है। कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो कभी सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 1981 से 2020 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल वर्षा, मृदा की नमी और भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है यह अनियमितता कृषि के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कृषि, अर्थव्यवस्था और मानव जीवन पर प्रभाव
जलवायु परिवर्तन का सबसे गहरा असर उत्तराखंड के ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जो मुख्यतः कृषि पर निर्भर है।
- कृषि पर संकट: पारंपरिक फसलें जैसे गेहूं, धान और मंडुवा (रागी) की पैदावार अनियमित वर्षा और सूखे के कारण प्रभावित हो रही है। किसानों को अपनी फसलों के लिए सिंचाई पर अधिक निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे उनकी लागत बढ़ रही है। कई स्थानों पर पानी की कमी के कारण किसानों को खेती छोड़नी पड़ रही है।
- जंगल की आग: गर्मियों में सूखे और बढ़ते तापमान के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। ये आग न केवल वनस्पति और वन्यजीवों को नष्ट करती हैं, बल्कि वायु प्रदूषण को भी बढ़ाती हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।
- स्वास्थ्य जोखिम: डॉ. गिरीश नेगी के अनुसार, वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन जैसी प्रदूषित गैसों का स्तर बढ़ने से लोगों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एलर्जी जैसी श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके अलावा, बदलते मौसम के पैटर्न से मलेरिया और डायरिया जैसे जल जनित और वेक्टर-जनित रोगों का खतरा भी बढ़ रहा है।
आपदाओं में वृद्धि और जैव विविधता का ह्रास. जलवायु परिवर्तन ने प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में भी वृद्धि की है।
- बाढ़ और भूस्खलन: अचानक भारी वर्षा और बादलों के फटने से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ और विनाशकारी भूस्खलन होते हैं। ये घटनाएं हर साल जान-माल का भारी नुकसान करती हैं और बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर देती हैं।
- जैव विविधता पर खतरा: बदलते तापमान और वर्षा के पैटर्न से वन्यजीवों और वनस्पतियों के प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहे हैं। कई पौधे और पक्षी अपनी भौगोलिक सीमा बदल रहे हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है। उदाहरण के लिए, कुछ पक्षियों की प्रजातियाँ जो पहले निचले इलाकों में नहीं पाई जाती थीं, अब वहां देखी जा रही हैं, जो उनके अस्तित्व के लिए खतरा है।
आगे का रास्ता: समाधान और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी इस गंभीर संकट से निपटने के लिए एक समन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- वन संरक्षण और वृक्षारोपण: हमें मौजूदा वनों की रक्षा करनी चाहिए और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने चाहिए। वन कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं।
- जल संरक्षण: जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और वर्षा जल संचयन (Rainwater harvesting) को बढ़ावा देना आवश्यक है। इससे पीने के पानी की कमी और कृषि पर निर्भरता को कम किया जा सकता है।
- कार्बन उत्सर्जन में कमी: व्यक्तिगत स्तर पर हमें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, ऊर्जा की बचत करनी चाहिए और नवीकरणीय ऊर्जा (जैसे सौर ऊर्जा) को बढ़ावा देना चाहिए।
- सतत कृषि: किसानों को जलवायु-अनुकूल फसलों और तकनीकों (जैसे जैविक खेती) को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- जागरूकता और शिक्षा: लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और इसे रोकने के तरीकों के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है।
यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम उत्तराखंड की इस अनमोल प्राकृतिक विरासत को बचाएं। सरकार और नागरिक दोनों को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और सुरक्षित उत्तराखंड में रह सकें।