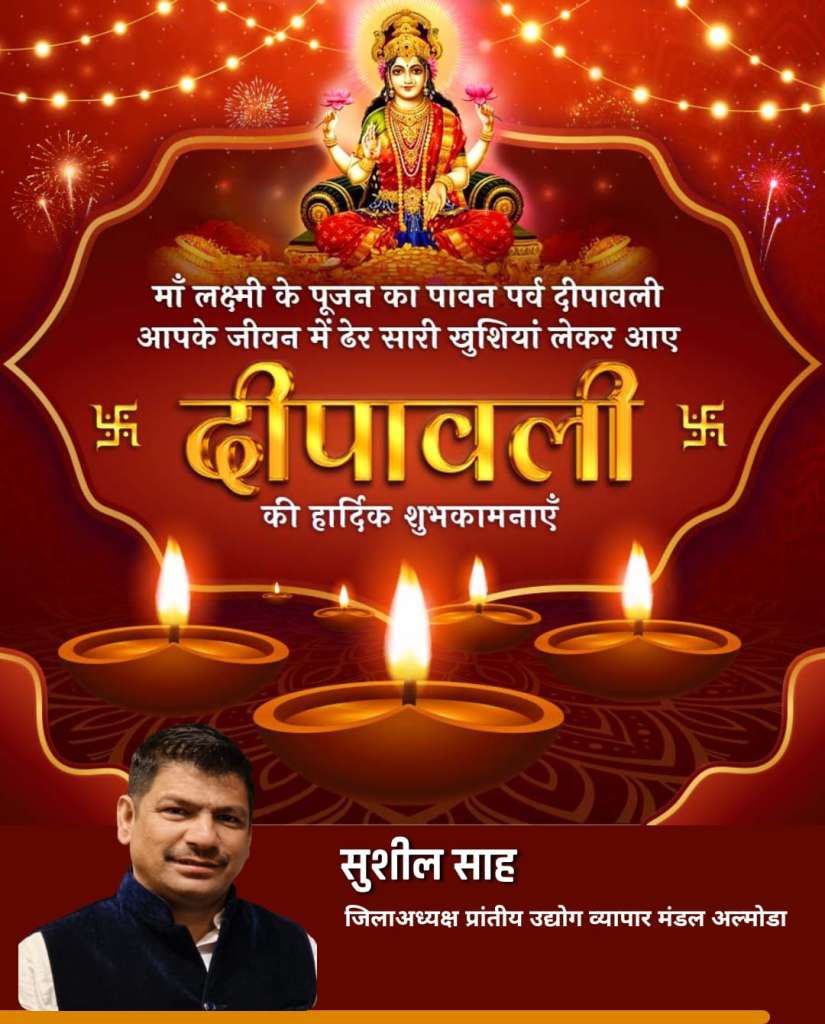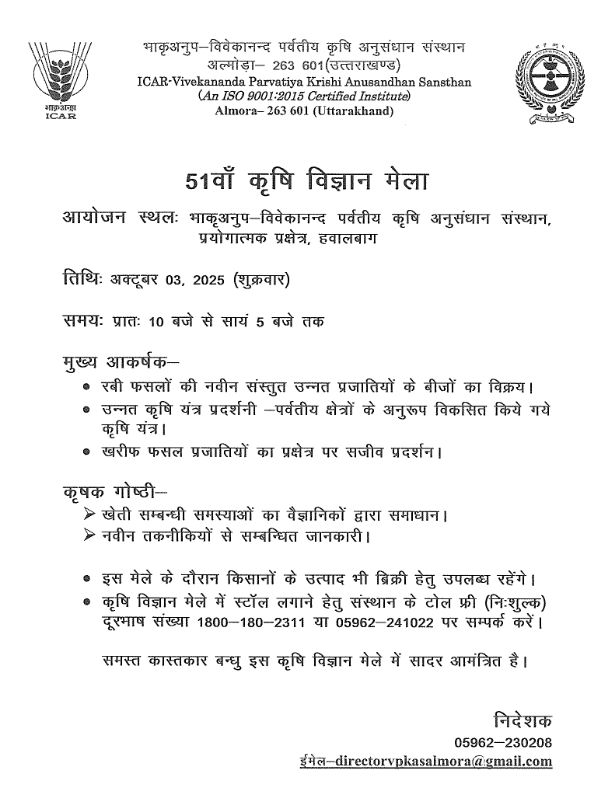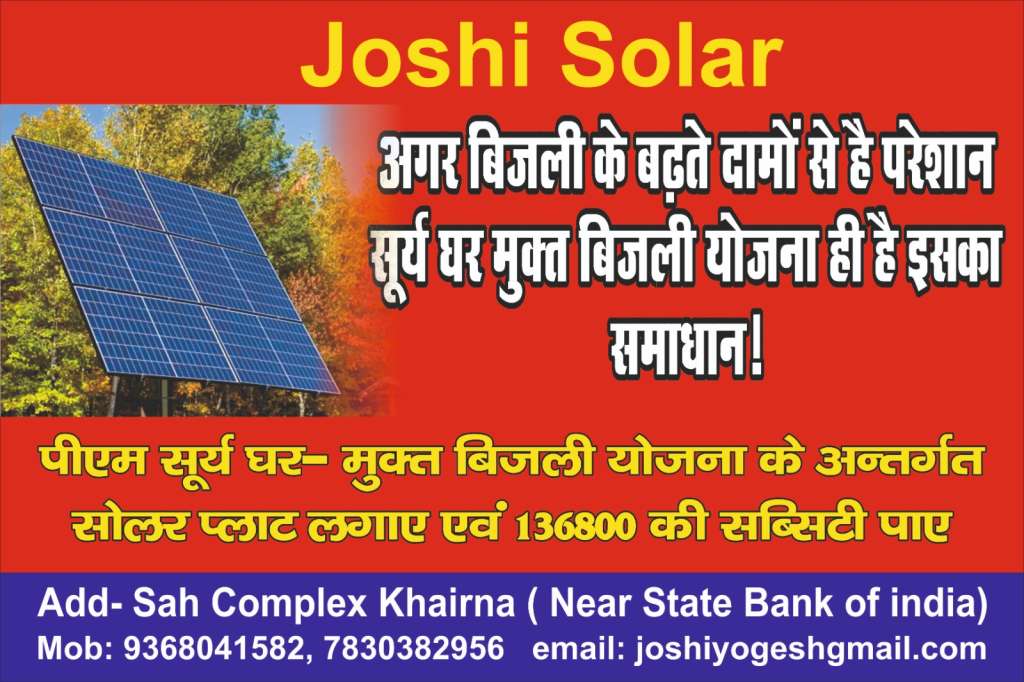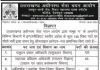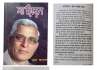जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (जीबीपी-एनआईएचई), कोसी-कटारमल, अल्मोड़ा में “भारतीय हिमालय क्षेत्र–2047 पर हिमालयन कान्क्लेव का शुभारंभ हुआ
( उद्घाटन सत्र में 75 विभिन्न संस्थानों के 200प्रतिभागियों ने 11राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेश से भाग लिया)“भारतीय हिमालय क्षेत्र–2047: पर्यावरण संरक्षण एवं सतत सामाजिक-आर्थिक विकास” विषय पर तीन दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव का शुभारंभ आज जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान (जीबीपी-एनआईएचई), कोसी-कटारमल, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में हुआ। यह कॉन्क्लेव जीबीपी-एनआईएचई द्वारा आयोजित किया गया है तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) सह-आयोजक है।
यह कार्यक्रम 13 से 15 नवम्बर 2025 तक चलेगा। कॉन्क्लेव का उद्देश्य विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप भारतीय हिमालय क्षेत्र (आईएचआर) के सतत विकास हेतु साझा दृष्टिकोण तैयार करना है।कॉन्क्लेव की मुख्य अतिथि थीं सुश्री नामिता प्रसाद, संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), भारत सरकार। विशेष अतिथियों में डॉ. लक्ष्मीकांत, निदेशक, वीपीकेएएस; प्रो. एस.पी.एस. बिष्ट, कुलपति, एसएसजे विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा; प्रो. साकेत कुशवाहा, कुलपति, लद्दाख विश्वविद्यालय; तथा प्रो. एस.पी. सिंह, पूर्व कुलपति, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय सम्मिलित थे।
उद्घाटन सत्र का आरंभ सम्मानित अतिथियों के स्वागत और “वंदे मातरम्” के सामूहिक गायन से हुआ। सत्र में हिमालयी राज्यों एवं संस्थानों से आए प्रख्यात वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया।अपने उद्घाटन भाषण में डॉ. आई.डी. भट्ट, निदेशक-प्रभारी, जीबीपी-एनआईएचई, ने कॉन्क्लेव का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि भारतीय हिमालय क्षेत्र भारत के लगभग 16% भू-भाग में फैला है, जिसमें दो जैव विविधता हॉटस्पॉट, 9,500 हिमनद (ग्लेशियर) और भारत की प्रमुख नदी प्रणालियाँ स्थित हैं, साथ ही यह क्षेत्र भारत की लगभग 30% जातीय विविधता को संजोए हुए है।
उन्होंने कहा कि इन प्राकृतिक संपदाओं के बावजूद यह क्षेत्र नाजुक और विकास की दृष्टि से पिछड़ा है। उन्होंने स्मरण कराया कि 1992 में जीबीपी-एनआईएचई द्वारा तैयार हिमालयन एक्शन प्लान ने सतत पर्वतीय विकास हेतु 10 विषयगत अनुसंधान क्षेत्रों की नींव रखी थी।डॉ. भट्ट ने कहा कि यद्यपि उल्लेखनीय प्रगति हुई है, परंतु जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और सामाजिक-पर्यावरणीय परिवर्तन जैसे उभरते मुद्दों पर समन्वित कार्यवाही की आवश्यकता है। विकसित भारत – 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप उन्होंने कहा कि कॉन्क्लेव का उद्देश्य जलवायु सहनशीलता और जैव विविधता संरक्षण को सुदृढ़ करना, सतत आजीविका एवं हरित अर्थव्यवस्था के अवसरों को प्रोत्साहित करना, शासन ढाँचों और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना तथा लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन को नीति और व्यवहार में मुख्यधारा में लाना है।
उन्होंने “हिमालय/माउंटेन एकेडमी ऑफ साइंसेज़” की स्थापना और “राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण रिपोर्ट” (IPCC मॉडल के अनुरूप) तैयार करने का प्रस्ताव रखा ताकि नीति निर्माण अधिक वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित हो सके। उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव में 75 से अधिक संस्थान, 13 हिमालयी राज्य व केंद्रशासित प्रदेश, तथा ICIMOD, IUCN, UNDP और WISA जैसे अंतरराष्ट्रीय सहयोगी भाग ले रहे हैं। उन्होंने विशेषज्ञों से आग्रह किया कि 1992 के हिमालयन एक्शन प्लान को वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप अद्यतन किया जाए। विशेष वक्तव्य में डॉ. लक्ष्मीकांत, निदेशक, आईसीएआर-वीपीकेएएस, अल्मोड़ा, ने कहा कि “विकसित भारत 2047 बिना विकसित हिमालय के संभव नहीं।” उन्होंने पश्चिमी हिमालय में घटते शुद्ध बोये क्षेत्र (net sown area) की चिंता जताई और विज्ञान-आधारित एकीकृत विकास रणनीतियों की आवश्यकता बताई जिससे संसाधन संरक्षण के साथ आजीविका सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।
प्रो. एस.पी.एस. बिष्ट, कुलपति, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, ने सामुदायिक आधारित इको-टूरिज्म की संभावनाओं पर बल दिया और कहा कि कॉन्क्लेव के निष्कर्षों को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि शोध और नीति के बीच बेहतर संबंध स्थापित हो। प्रो. साकेत कुशवाहा, कुलपति, लद्दाख विश्वविद्यालय, ने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल हरित एवं पुनर्जनन तकनीकों के विकास की आवश्यकता बताई और कार्बन क्रेडिट, विकिरण प्रभाव तथा वेस्ट-टू-वेल्थ नवाचारों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने का सुझाव दिया।
प्रो. एस.पी. सिंह, पूर्व कुलपति, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, ने हिमालय की भूवैज्ञानिक नाजुकता पर प्रकाश डालते हुए अंतर-देशीय (transboundary) शोध नेटवर्क विकसित करने का सुझाव दिया जिससे ज्ञान-साझेदारी और सामूहिक समाधान को बढ़ावा मिल सके। मुख्य अतिथि सुश्री नामिता प्रसाद, संयुक्त सचिव, MoEF&CC, भारत सरकार ने जीबीपी-एनआईएचई की हिमालयी अनुसंधान एवं विकास प्राथमिकताओं में मार्गदर्शक भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि कॉन्क्लेव के निष्कर्षों को राज्य और राष्ट्रीय नीतियों में समाहित किया जाना चाहिए। उन्होंने जीबीपी-एनआईएचई द्वारा प्रस्तुत हिमालय-विशिष्ट वैज्ञानिक अकादमी और “राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण रिपोर्ट” की प्रस्तावना की सराहना की।सत्र का समापन जीबीपी-एनआईएचई, हिमाचल क्षेत्रीय केंद्र, कुल्लू के वैज्ञानिक-एफ ई.आर. आर.के. सिंह द्वारा प्रस्तुत आभार प्रस्ताव के साथ हुआ। उन्होंने सभी अतिथियों, सहयोगी संस्थानों और प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।कॉन्क्लेव में कुल पाँच पूर्ण सत्र और सोलह समानांतर सत्र तीन दिनों में आयोजित होंगे।
पूर्ण सत्रों में “भारतीय हिमालय क्षेत्र 2047 – विकसित भारत की दिशा में संभावनाएँ और चुनौतियाँ”, “सतत समाधान हेतु पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण”, “हिमालय युवा शोधकर्ता मंच – भविष्य हेतु हिमालय को जोड़ना”, “लैंगिक समानता एवं सामाजिक समावेशन – नीति एवं व्यवहार में मुख्यधारा बनाना” और “विज्ञान–नीति–व्यवहार का एकीकरण” जैसे विषय शामिल हैं। समानांतर सत्रों में “पर्यावरणीय नाजुकता–नगरीकरण और अवसंरचना”, “जैव विविधता–वर्तमान परिदृश्य और संभावनाएँ”, “सतत जल संसाधन प्रबंधन”, “प्राकृतिक संसाधन आधारित आजीविका समाधान”, “पर्यावरणीय स्थिरता–प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन”, “जैव विविधता–संरक्षण और प्रबंधन”, “पर्वतीय कृषि का पुनःदृष्टिकरण”, “स्वदेशी ज्ञान और लचीलापन निर्माण”, “आपदा जोखिम न्यूनीकरण–जलवायु चरम और प्राकृतिक आपदाएँ”, “मानव–वन्यजीव सह-अस्तित्व और संघर्ष प्रबंधन”, “आर्द्रभूमि और पीटलैंड प्रबंधन–बदलते जलवायु में विवेकपूर्ण उपयोग”, “पर्वतीय कृषि-तंत्र में वास्तविक मूल्यांकन (True Value Accounting)”, “क्षेत्रीय सहयोग–परिदृश्य पुनर्स्थापन और प्रबंधन”, “पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ–संरक्षण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन”, “हरित ऊर्जा–कार्बन न्यूट्रल समाधान” तथा “सतत पर्यटन–पर्यावरणीय, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों में संतुलन” जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी।कॉन्क्लेव के आगामी दो दिनों में जलवायु सहनशीलता, जैव विविधता संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत आजीविका जैसे विषयों पर सत्र आयोजित होंगे, जिनका उद्देश्य भारतीय हिमालय क्षेत्र के लिए एक सशक्त और समृद्ध भविष्य का निर्माण करना है। उद्घाटन सत्र में 75 विभिन्न संस्थानों के लगभग 200 प्रतिभागियों ने 11 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों से भाग लिया।